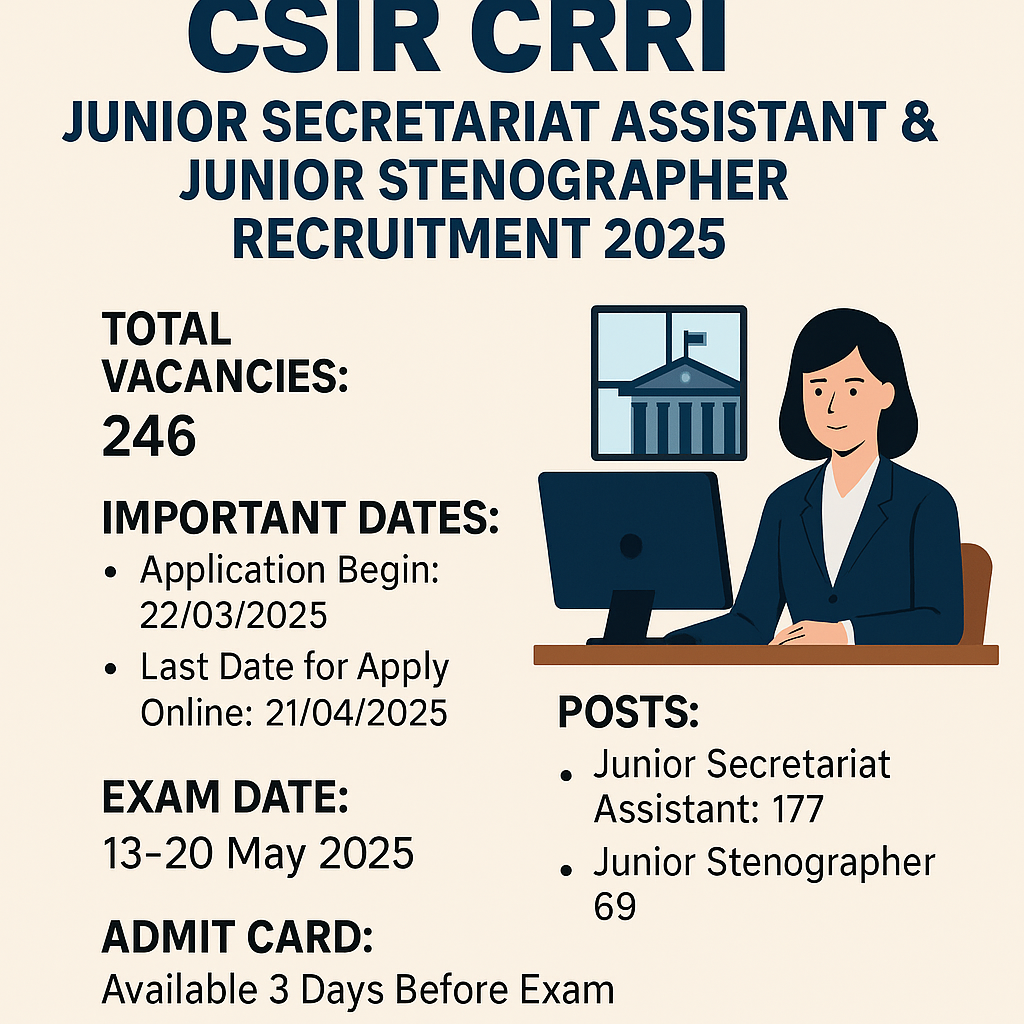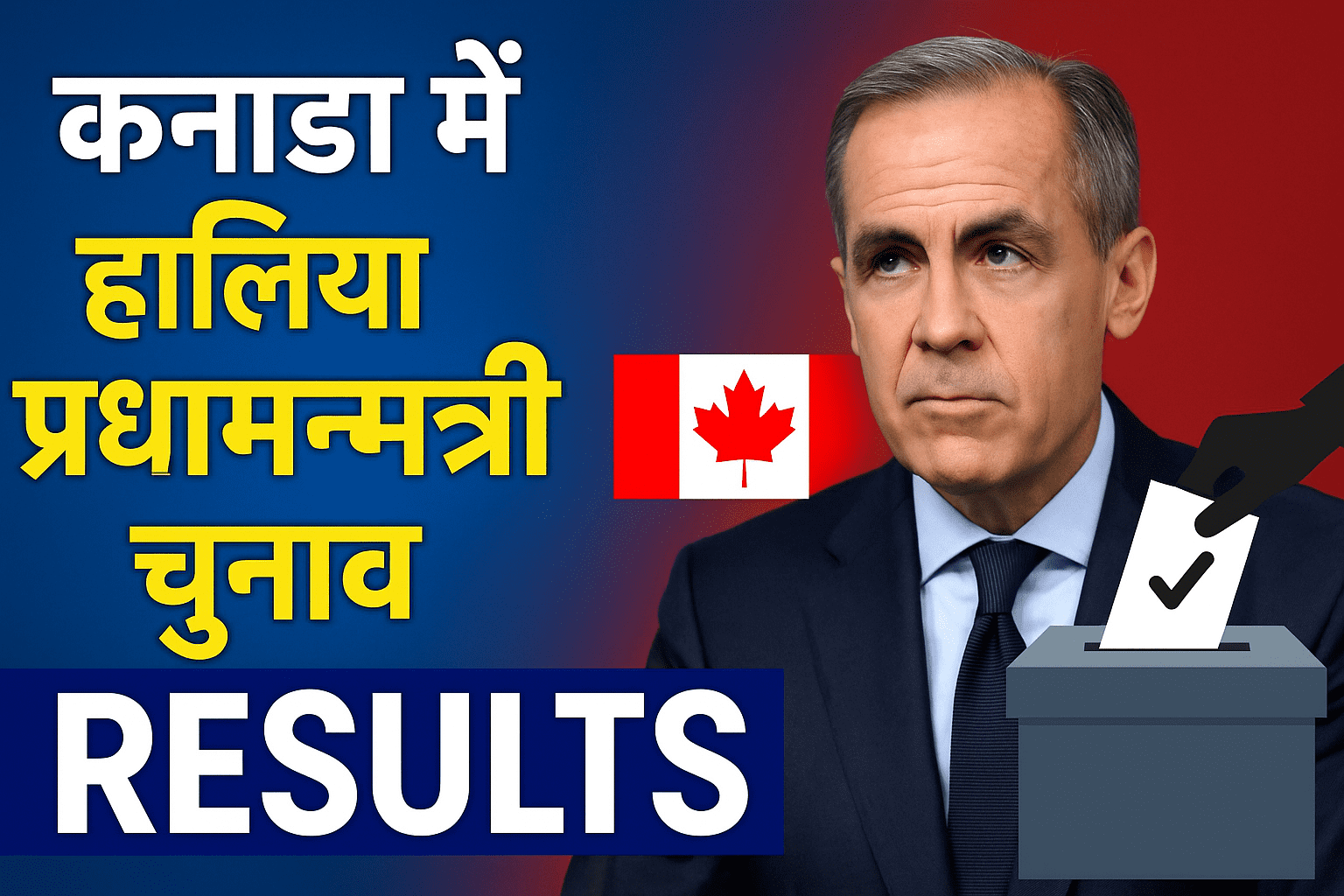1. उपनिवेशकालीन आरंभ (1871–1931)
- 1871–72: ब्रिटिश शासन के तहत पहली बार पूरे उपनिवेश में जनगणना कराई गई, जिसमें लोगों की जाति‑वर्गीकरण का भी विवरण शामिल था। उदाहरण के लिए बॉम्बे प्रेसीडेंसी में ब्राह्मण, क्षत्रिय/राजपूत, वैश्य और शूद्र समूहों की आबादी दर्ज की गई।
- 1881–1931: हर दस साल पर होने वाली इन गणनाओं में जातिगत आंकड़े लगातार बटोरते रहे।
- 1931: स्वतंत्रता से पहले हुई अंतिम जाति‑आधारित जनगणना के अनुसार कुल आबादी का लगभग 52% हिस्सा ‘अन्य पिछड़े वर्ग’ (OBC) का था, और देशभर में करीब 4,147 अलग-अलग जातियाँ/उपजातियाँ गिनाई गईं। बाद में मंडल आयोग ने इसी आंकड़े को आधार बनाकर OBC को 27% आरक्षण देने की अनुशंसा की।
2. युद्धकालीन और बाद के दशक (1941–2011)
- 1941: द्वितीय विश्व युद्ध के बीच अनुमानित रूप से हुई गणना में भी जातिगत आंकड़े जुटाए गए, लेकिन यह विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ।
- 1951–2011: आज़ाद भारत में हर दस साल पर कुल जनगणना तो होती रही, लेकिन जाति‑वर्ग के विस्तृत विवरण केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) तक सीमित रह गए। अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) या अन्य समुदायों का अलग‑अलग फैली हुई जानकारी शामिल नहीं की गई।
3. सामाजिक‑आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) और राज्य‑स्तरीय सर्वेक्षण (2011–2023)
- 2011 (SECC): यूपीए सरकार ने “सामाजिक‑आर्थिक एवं जाति जनगणना” आयोजित की, जिसमें घरों की आर्थिक हालत के साथ‑साथ जातिगत पहचान भी दर्ज करने का प्रयास हुआ। हालांकि विस्तृत OBC/अन्य वर्ग के आँकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन घरों द्वारा खुला प्रश्न भरने पर लगभग 46 लाख अलग-अलग जाति‑नाम आए।
- 2022–23 (राज्य‑स्तरीय सर्वे): बहुतेरे राज्यों ने स्वैच्छिक रूप से जाति सर्वे संपन्न किए।
- बिहार (2022): OBC+EBC का संयुक्त हिस्सा लगभग 63% माना गया।
- तेलंगाना (2023): पिछड़े वर्ग (BC) की जनसंख्या 56% पाई गई।
- कर्नाटक (2015 में सर्वे, परिणाम 2023 में): OBC का हिस्सा लगभग 70% आंका गया।
4. आगामी जनगणना और उसकी संभावित दिशा (2025)
- केंद्र सरकार ने मई 2025 में घोषणा की कि कोविड‑19 के कारण टली हुई 2021 की जनगणना में अब जातिगत प्रश्न दोबारा शामिल किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पुष्टि की है कि अगली गणना में जाति‑वर्ग के आंकड़े एकत्रित होंगे।
5. सामाजिक‑राजनीतिक प्रभाव
- 1931 के OBC आंकड़ों ने ही मंडल आयोग की सिफारिशों को बल दिया और शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण का रास्ता बनाया।
- हाल के राज्य‑स्तरीय सर्वेक्षणों ने आरक्षण की वर्तमान सीमा (50%) पर बहस तेज कर दी है—विशेषकर कर्नाटक में जहाँ OBC 70% पाए जाने पर कुछ हिस्सों ने कोटा बढ़ाने की मांग की।
- जातिगत जनगणना का राजनीतिककरण भी देखने को मिला है: कांग्रेस लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर समग्र जाति‑गणना की मांग करती आ रही है, जबकि दूसरी तरफ भाजपा ने इसे चुनावी रणनीति के रूप में उपयोग करने के आरोपों के बीच आखिरकार समर्थन कर दिया है।
मई 2025 में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक रूप से यह निर्णय लिया है कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में पहली बार जातिगत आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। इसका उद्देश्य लंबे समय से आयामहीन रणनीतियों पर आधारित आरक्षण और कल्याण योजनाओं को वास्तविक जनसंख्या डेटा पर आधारित बनाना है। इस पहल के पीछे प्रमुख रूप से विपक्षी दलों और राज्यों द्वारा उठाई गई मांगों के साथ-साथ पिछड़े वर्गों की वास्तविक हिस्सेदारी उजागर करने के उद्यमों का योगदान है।
पिछली पहलों का आकलन
2011 में आयोजित सामाजिक‑आर्थिक जाति सर्वेक्षण में तकरीबन सभी जातियों की सूची तैयार तो हुई थी, लेकिन उसमें तकनीकी खामियां और डेटा की गोपनीयता ने व्यापक विश्लेषण को सीमित कर दिया। बाद में कई राज्यों ने अपनी श्रृंखला में सर्वेक्षण कराए, जिनमें कुछ स्थानों पर ओबीसी आबादी दोहरे अनुमान तक पहुंची। इन परिणामों ने राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता की कमी को उजागर किया और समुचित हस्तक्षेप की मांग और तेज कर दी।
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
विपक्षी दलों ने इस निर्णय को अपनी लगातार मांगों की सफलता के रूप में पेश किया है, वहीं सत्ताधारी गठबंधन इसे एक सामूहिक सामाजिक हित की जरूरत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, आने वाले चुनावी परिदृश्य में यह आंकड़ा-आधारित कदम नीतिगत संतुलन बनाने और चुनावी रणनीतियों को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
आरक्षण नीति पर पुनर्विचार: राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी, एससी-एसटी आदि वर्गों की वास्तविक जनसंख्या का आंकड़ा मिलने के बाद आरक्षण की प्रतिशत सीमा और उसकी आवश्यकता पर व्यापक बहस छिड़ सकती है।
योजनाओं का लक्ष्यीकरण: कल्याण योजनाओं को अब स्टैक किए गए अनुमानों पर नहीं, बल्कि ताज़ा जनगणना डेटा पर आधारित किया जा सकेगा, जिससे वंचित तबकों को लाभ की संभावना बढ़ेगी।
चुनावी समीकरण: जातिगत बैंकिंग पर निर्भर दलों को नई जनसांख्यिकी के अनुरूप अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी; इससे चुनावी अलायंस और एजेंडे में बदलाव की सम्भावना है।
प्रावधानात्मक चुनौतियां
जातियों के मानकीकरण, स्थानीय उप-समूहों की पहचान और व्यापक डेटा संग्रहण की प्रक्रिया जटिल है। विशेषज्ञ इस बात पर संकेत दे रहे हैं कि सैकड़ों विविध जातियों को राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकृत और समेकित करना प्रशासनिक और तकनीकी दोनों दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण होगा।
राज्यों के अनुभव
विभिन्न राज्यों में किए गए सर्वेक्षणों ने इस फैसले को गति दी है:
- कुछ प्रांतों में पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी 55–70% के बीच पाई गई, जो पहले के अनुमान से दोगुनी से भी अधिक थी।
- इन परिणामों ने स्थानीय स्तर पर आरक्षण बढ़ाने और योजनाओं में संशोधन की सलाह दी, जिससे केंद्र पर भी दबाव पड़ा।